भारतीय समाज में कुछ ऐसे लोग निवास करते हैं जो सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करके उत्थान का प्रयास की आवश्यकता होती हैं। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 में कुछ ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके उनका अलग नामकरण किया गया हैं। जिसे 'अनुसूचित क्षेत्र' और 'जनजातीय क्षेत्र' कहा गया।
पाॅंचवी अनुसूची में इनके प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गयी हैं।
जो सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामाजिक समूह हैं, उन्हीं आदिम निवासी माना गया हैं। इनकी जिन राज्यों में अधिक संख्या हैं। उन राज्यों को अनुसूचित किया गया हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में पाॅंचवी अनुसूची में राज्यों को भी अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हैं। लेकिन पाॅंचवी अनुसूची में पूर्वोत्तर के राज्य - असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम की चर्चा नहीं हैं। इन पूर्वोत्तर के चार राज्यों की चर्चा छठी अनुसूची में की गई हैं।
दूसरे सामान्य राज्यों की तुलना में अनुसूचित क्षेत्रों के साथ भिन्न रूप में व्यवहार किया जाता है क्योंकि वहांँ आदिम निवास करते हैं। यही आदिम सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। इन्हीं के सामाजिक व आर्थिक स्थिति को सुधार व अच्छा करने के लिए भारतीय संविधान के कई अनुच्छेदों में प्रावधान किये गये हैं। जिसे हम आगे अध्ययन करेंगे। वर्तमान आदेश- 2016 के अनुसार भारत के 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं। जैसे- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों में निवास करने वाली आदिम निवासियों के सामाजिक व आर्थिक स्थिति को सुधारने व अच्छा करने के लिए विशेष रूप से भारतीय संविधान में प्रावधान किए गए हैं। साथ-ही-साथ इनके विकास के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाये गये हैं जो एक संवैधानिक आयोग हैं।
जनगणना - 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या 8 करोड़ 43 लाख, लिंगानुपात 957/1000, साक्षरता दर 59 फीसदी, काम करने का दर 48.7 फीसदी प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल जाने वाले बच्चों कि 15.29 फीसदी, लोकसभा में आरक्षित सीट 47 और विधानसभा में 554 सीट आरक्षित हैं।
अनुसूचत जनजाति की वर्तमान स्थिति (Current status of scheduled tribe) –
भारत की कुल आबादी का 8.14% और कुल क्षेत्रफल का 15% भाग पर आदिवासी निवास करते हैं। आदिवासी कुल आबादी का 52% गरीब रेखा के नीचे जीवन बसर करते हैंं। कुल आदिवासी जनसंख्या का 54% आज भी आर्थिक सम्पदा जैसे संचार और परिवहन तक पहुंँच नहीं पाए हैं। अनुसूचित जनजातियों (आदिवासियों) की कोई ठोस परिभाषा नहीं दी जा सकी हैं। इन्हें अनुच्छेदों में वर्णित शब्दों के आधार पर ही जानते हैं। जैसे- अनुच्छेद- 366 (25) अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में जाना जाता हैैंं। वह अनुच्छेद- 342 के अनुसार हैं। जिसमें कहा गया है कि आदिवासी समुदाय या आदिवासी समूह हैैंं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया हैं। जो मुख्य रूप से वनों और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैंं। ये सामााजिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं।
अनुसूचित जनजातियों के खास विशेषताएं (Special features of Scheduled Tribes) —
- सरल व सादगी से जीवन यापन
- निश्चल स्वाभाव
- भौगौलिक अलगाव
- हर जनजाति की अपनी एक संस्कृति होती है
- प्रकृति प्रेमी
- बाहरी समुदाय के साथ सम्पर्क में संकोच
- आर्थिक रूप से पिछड़ापन
- अपने समुदाय में मुखर
- सामाजिक रुप से संगठित
- माहसत्तात्मक और विहसत्तात्मक परिवार
- पिहसत्तात्मक परिवार अधिक प्रभावी
- जनजाति का अपना एक नाम होता है
- जनजाति का अपना एक राजनीतिक संगठन होता हैं
- जनजाति का स्वतंत्र सुरक्षात्मक संगठन होता है
- वितरण एक सुनिश्चित भूभाग पर होता है
- जनजाति की अपनी एक भाषा होती है
- गोत्र और अंतर्विवाही समूहों की विशिष्टता होती है
- जनजाति परिवारों का समूह है आदि।
प्रमुख जनजातियों के नाम (Names of major tribes) –
- संथाल
- मुण्डा
- उराँव
- हो
- भूमिज
- लोधा
- कोया
- खोण्ड
- गोंंड
- सोवर
- गदवा
- कमार
- बैगा
- भूईवाँ
- कोरकू
- हल्वा
- गद्दी
- गुज्जर
- भोट
- किन्नौरा
- थारू
- कुकी
- मिजो
- कचारी
- हमार
- बिमसा
- नागा
- रियान
- थडा़ऊ
- मीना
- भील
- डफली
- घोटिया
- गमीत
- सह्याद्रि
- कोली
- महादेव
- कोंकण
- कोया
- अण्डी
- मेरूकूूलू
- कोण्डा-डोरा
- इरूला
- माला
- कुरावन
- नैैैकाड़़ा
- यरावा
- पुुुलियन
- पनियन
- कादर
- अण्डमानी
- ओंगे
- जरावा
- शाँम्पेेन
- सेन्टेनेलिस, आदि।
जनजातियों के संबंध में कुछ विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से परिभाषा भी दी हैं। जिसे हम निम्नलिखित विद्वानों द्वारा दी गयी परिभाषा को देखेंगे –
रेमण्ड फर्थ- "जनजाति एक ही सांस्कृतिक श्रृंखला का मानव समूह है जो साधारणतः एक ही भूूू-खण्ड पर रहता है, एक भाषा-भाषी हैं तथा एक ही प्रकार की परम्पराओं एवं संस्थाओं का पालन करता हैैं और एक ही सरकार के प्रति उत्तरदायी होता हैं।"
जार्ज पीटर मर्डाक- "यह एक सामाजिक समूह होता हैै जिसकी एक अलग भाषा होती है तथा भिन्न संस्कृति व एक स्वतंत्र राजनैतिक संगठन होता हैं।"
डब्लू॰ एच॰ आर॰ रिवर्स- "जनजाति एक सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसकी सामान्य भाषा है तथा जो युद्ध जैसी विपत्तियों का संगठित रूप से सामना करती हैैं।
रिवर्स इसमें सामान्य निवास को महत्वपूर्ण नहीं मना है क्योंकि अनेक जनजातियों घुमन्तू होती हैं।
फ्रेंच बोआस- "जनजाति का अर्थ आर्थिक दृष्टि सेे ऐसा स्वतंत्र जन-समूह है जो एक भाषा बोलता है और वाह्य आक्रमण सेे सुरक्षा के लिए संगठित होता हैैं।"
गिलिन और गिलिन- "जनजाति किसी भी ऐसे स्थानीय समुदायों के समूह को कहा जाता है जो एक सामान्य भूू-भाग पर निवास करता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो, और एक सामान्य संस्कृति का व्यवहार करता हो।"
डी॰एन॰ मजूमदार- "जनजाति को 'परिवारों' का संकलन कहा है जिसका अपना एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूू-भाग पर रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं, विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में कुछ निषधों का पालन करतेेे हैं तथा एक सुनियोजित आदान प्रदान की व्यवस्था का विकास करते हैं।"
इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार, "जनजाति ऐसे परिवारों का संकलन है जिसका एक सामान्य नाम है, सामान्य भाषाा है तथा जो सामान्य भूू-भाग में बसे हुुुए हैं अथवा उसमें बसेेे होने का दवा करते हैं तथा वे प्रायः अन्तर्विवाही नहीं होते हैं, चाहे पहले ऐसी प्रथा उनमें पायी जाती रही हो।"
उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं की जनजाति की परिभाषा के संबंध में विद्वानों में मतैक्यता का अभाव हैं। जनजाति की एक स्थूल परिभाषा नहीं दी जा सकती। क्योंकि भौगोलिक विविधता, जनजातियों के विभिन्नता, संस्कृति व व्यवहार के कारण उनकी परिभाषाओं में भी विभिनता पायी जाती हैं।
जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकास के लिए भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन् 1950 में जनजातियों की पहचान करके 212 जनजातीय समुदायों की सूची तैयार करने के बाद अनुसूचित जनजातीय आदेश - 1950 में लागू किया गया था। इन्हीं सूचीबद्ध जनजातियों को ही 'अनुसूचित जनजाति' कहा गया। अभी भी बहुत-सी जनजातीय समुदाय इस सूची में शामिल नहीं हो पाये हैं।
भारतीय संविधान निर्माताओं ने उनके इनके अविकसित रूप को ध्यान में रखकर जनजातियों को विशेष महत्व देते हुए इनके विकास के लिए भारतीय संविधान में विभिन्न भागों और अनुच्छेदों में विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई हैं। भारतीय संविधान के भाग-3, भाग-4, भाग-10, भाग-12, भाग-16 को विकास के लिए अनिवार्य माना गया है जिसे हम अध्ययन के क्रम में आगे देखेंगे।
इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की भाषा एवं शब्दों की दृष्टि से जनजातीय भारत के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्व॰ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनजातियों के विकास के लिए पांच मूल सिद्धांतों के बारे में विचार किया था-
- लोगों को अपनी तरक्की अपनी मनपसंद राह पर अपनी "जीनियस" के मुताबिक करनी चाहिए और हमें भरसक किसी भी चीज को उन पर लादने से परहेज करना चाहिए।
- जमीन और जंगलात पर जनजातियों के सनातन हक का आदर होना चाहिए।
- विकास और प्रशासन को प्रशिक्षित करना चाहिए।
- तरक्की की बहुत सारी स्कीमों और अतिप्रशासन से बचाना चाहिए और
- आखरी नतीजे पर जोर करते वक्त हमें आंकड़ों और लागत की रकमों की जगह आदमी के चरित्र के विकास का लेखा-जोखा लेना चाहिए।
जनजातीय विकास हेतु भारत सरकार द्वारा प्रयास (Efforts by the Government of India for tribal development) –
भारत में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग पहली बार शासन अधिनियम 1935 में किया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जाति का निर्धारण किया गया इसके आधार पर संबंधित राज्यों के राज्यपाल से भी परामर्श किया जाता रहा हैं। इसके अनुसार अनुसूचित जनजाति का मतलब आदिवासी अथवा वनवासी समुदाय से है जो भौगोलिक रूप से सुदूर पहाड़ी एवं अन्य क्षेत्रों में रहते हैं। यह आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से अत्यधिक पिछड़े हुए हैं और अपनी आजीविका के लिए पूर्णता व अन्य उत्पादों व कृषि पर निर्भर रहते हैं।
अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए भारत सरकार ने कई प्रकार के उपाय किए हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इनके विकास के लिए विभिन्न आयोग एवं कमेटियां गठित की गई जिनमें से प्रमुख आयोग एवं कमेटियों को निम्नलिखित ढंग से देख सकते हैं -
- पिछड़ा वर्ग आयोग प्रतिवेदन - 1955
- समाज कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण अध्ययन टीम का प्रतिवेदन - 1959
- संसद पूर्वानुमान समिति का 40वाँ प्रतिवेदन - 1959
- बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खण्ड समिति का प्रतिवेदन - 1960
- अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रतिवेदन - 1960 - 61
- ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु अध्ययन समूह का प्रतिवेदन - 1961
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति रोजगार पर आयोजित सेमिनार का प्रतिवेदन - 1964
- वन-क्षेत्रों में जनजातीय अर्थव्यवस्था समिति का प्रतिवेदन - 1964
- जनजातीय विकास कार्यक्रम समिति का प्रतिवेदन - 1969
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण हेतु गठित संसदीय समिति का प्रतिवेदन - 1972
- जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु गठित टास्कफोर्स समिति का प्रतिवेदन - 1972
- जनजातीय विकास हेतु विशेषज्ञ समिति प्रतिवेदन - 1972
- 65वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग - 1990 (जनजातीय आयोग - 2004 से प्रभाव में आया)
- जनजातीय मंत्रालय - 1999.
जनजातियों के विकास हेतु बनाए गए आयोग के 6 क्षेत्रीय कार्यालय बनाये गये। जिससे विकास कार्यों को आसानी से धरातल पर उतारा जा सके। ये छः क्षेत्रीय कार्यालय 6 राज्यों में बनाये गये –
- भोपाल (मध्य प्रदेश)
- भुवनेश्वर (उड़ीसा)
- जयपुर (राजस्थान)
- रायपुर (छत्तीसगढ़)
- रांँची (झारखण्ड)
- शिलांग (मेघालय)।
उक्त प्रतिवेदनों द्वारा प्रेषित सुझावों को जनजातीय विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सरकारें लागू करती रही हैं। इस विकास कार्य को अब नीति आयोग के माध्यम से किया जा रहा हैं। यह नीति आयोग - 2015 से अस्तित्व में आया हैं। विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की राशि बढ़ती भी रही हैं। जैसे –
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) में 22.22 करोड़
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956 - 61) में 48.86 करोड़
तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961- 66) में 52.55 करोड़
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969 -74) में 75.00 करोड़
पंचम पंचवर्षीय योजना (1974 -79) में 105.00 करोड़
इसी प्रकार अगली पंचवर्षीय योजनाओं एवं नीति आयोग के माध्यम से विकास कार्यों की राशि बढ़ती गयी।
भारत में विभिन्न प्रकार के समस्याओं से घिरे होने के बावजूद भी जनजातियों में अपनी अस्मिता व स्वतंत्रता के लिए कई आन्दोलन व विद्रोह भी किये। कई ऐसे आन्दोलन हुए, जिसमें हिंसा भी हुई। कई आदिवासी नेता मौत के घाट उतार दिये गये। जनजातियों द्वारा किये गये, प्रमुख आन्दोलन जो ब्रिटिश सल्तनत के समय हुई –
1. तत्कालीन बिहार (अब झारखण्ड) के रांँची जिला में –
- तमन विद्रोह – (1789,1794 - 95)
- छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह – (1807-1808)
- मुण्डा विद्रोह – (1820 - 32)
- भूमि रोक विद्रोह – (1858 - 59)
- सरदार आन्दोलन – (1869 - 80)
- अंग्रेजों के विरोध में मुण्डा सरदार आन्दोलन – (1889)
- बिरसा आन्दोलन – (1890 - 99)
- ताना भगत आन्दोलन – (1920 - 21)।
2. संथाल परगना में –
- संथाल विद्रोह – (1855)
- ग्रामीण विद्रोह – (1871-72)
- भागीरथ आन्दोलन – (1874 -75)
- दूबिया गोंसाई आन्दोलन – (1880 - 81)।
3. मध्य भारत में –
- चकरा बिसोई आन्दोलन (उड़ीसा) – (1850)
- नायक दास का विद्रोह (गुजरात) – (1858)
- तमनदोरा के नेतृत्व में कोया विद्रोह (उड़ीसा) – (1880)
- बस्तर जनजातीय विद्रोह (मध्य-प्रदेश) – (1911)
- लक्षमन नायक का कोरापुत विद्रोह (उड़ीसा) – (1942)
- राजा मोहिनी देवी सामाजिक आर्थिक सुधार आन्दोलन (मध्य-प्रदेश) – (1951)।
4. उत्तरी-पूर्वी भारत में –
- खम्पटी विद्रोह (असम) – (1839)
- नागा विद्रोह – (1879)
- जेलियांग रोज आन्दोलन – (1917-1932)।
5. आंध्र प्रदेश में –
- कोया मुत्तदार आन्दोलन – (1862 - 1879)
- रम्पा विद्रोह –(1922)
- गोंड एवं कोलम विद्रोह – (1941) में हुए थे।
उपर्युक्त अध्ययन से ज्ञात होता है कि जनजातियों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और अलगाव की स्थिति अच्छी नहीं रहने के बावजूद भी अपनी अस्मिता, स्वतंत्रता और ब्रिटिश सल्तनत के गलत नीतियों के खिलाफ एकजुटता के साथ कई आन्दोलन किये। जिसमें रक्तपात भी हुआ। इससे पता चलता है कि जनजातीय लोग स्वाभिमानी होते हैं। अपनी सभ्यता व संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने वालों को बकसते नहीं हैं। उनका डटकर एकजुटता के साथ विरोध करते हैं। ये शांत प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। अगर इनके स्वाभिमान पर कोई आघात करता है तो ये हिंसक भी हो जाते हैं। अपनी मातृभूमि से प्यार करने वाले होते हैं। तभी तो अभी तक इन पर किसी प्रकार का लाक्षण नहीं लगा। मातृभूमि से प्यार और इनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने इनके उत्थान व विकास के लिए संविधान में कई प्रकार की व्यवस्थाएंँ की हैं और इन व्यवस्थाओं के माध्यम से जनजातीय समुदाय को विकसित किया जा रहा हैं। फलतः भारत के जनजातीय समुदाय अब धीरे-धीरे समाज के मुख्य धारा में शामिल हो भी रहे हैं।


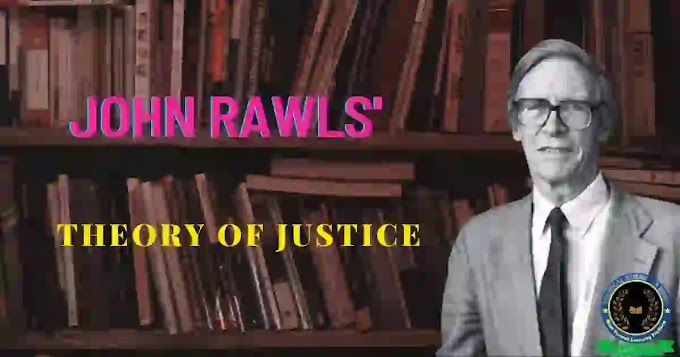
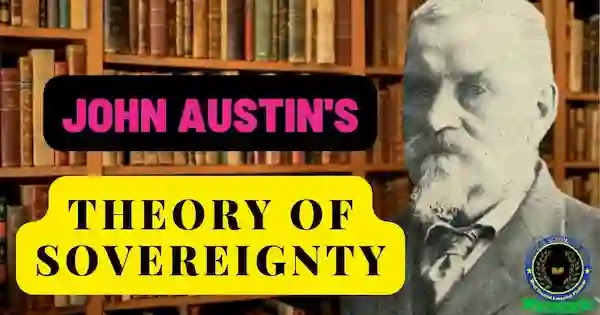
.webp)

0 टिप्पणियाँ
If you have any doubts, Please let me know