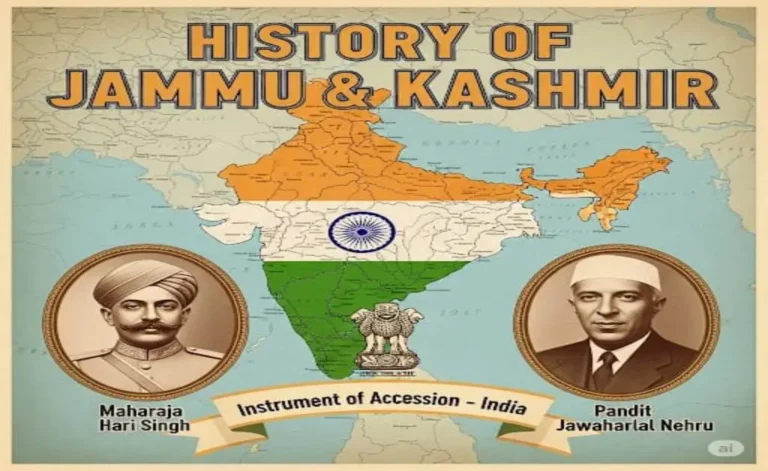What Is Citizenship – नागरिकता क्या हैं?
राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति, जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है तथा वह अपने राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता है, नागरिकता (Citizenship) कहलाता हैं।
नागरिकता (Citizenship
) किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है, जिसमें उसे नागरिक के रूप में वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं, जो संविधान द्वारा निर्धारित किए गये हैं। ये अधिकार किसी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। किसी भी राज्य की जनसंख्या को दो भागों में विभाजित किया जाता हैं–
नागरिक और गैर-नागरिक। नागरिकों को सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, किंतु गैर-नागरिकों को ये अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं। नागरिक अपने राजनीतिक समूह के सदस्य होते हैं। यही मिलकर राज्य का गठन करते हैं।
नागरिकता मुख्य रूप से चार प्रकार की होती हैं –
- राष्ट्रीय नागरिकता।
- अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता।
- राष्ट्रमण्डलीय नागरिकता और
- मानद नागरिकता।
हम यहांँ राष्ट्रीय नागरिकता के बारे में समझेंगे। नागरिकता की अवधारणा पहले कानूनों से उत्पन्न हुई।
नागरिकता की ऐतिहासिक पहलू –
पोलिस (प्राचीन यूनान के नगर-राज्य) नागरिकता इस बात पर आधारित थी कि लोग पोलिस के छोटे पैमाने के कार्बनिक समुदायों में किस तरीके से प्राचीन यूनानी काल में रहते थे। उन दिनों में नागरिकता को एक सार्वजनिक मामले के रूप में नहीं देखा जाता था, यह एक व्यक्ति के निजी जीवन से अलग होती थी। नागरिकता के दायित्व पोलिस के दैनिक जीवन के साथ गहराई से जुड़े थे। सही मायने में मनुष्य होने के लिए, व्यक्ति को समुदाय का एक सक्रिय नागरिक बनना पड़ता था। अरस्तु के शब्दों में “समुदाय के मामलों के संचालन में हिस्सा न लेने का अर्थ है कि या तो आप जानवर हैं या देवता” पोलिश के नागरिक दायित्वों को धार्मिक होने का अवसर मानते थे, यह उनके लिए सम्मान और आदर का एक स्रोत होता था। एथेंस में, शासक और शासित दोनों प्रकार के नागरिक थे, महत्वपूर्ण राजनीतिक और न्यायिक कार्यालयों को चलाया करते थे। सभी नागरिकोंं को राजनीतिक सभा में बोलने और मतदान करने अधिकार होता था। लेकिन यह अधिकार नागरिकों को ही प्राप्त थे। गैैर-नागरिकों को नहीं। नागरिकोंं का स्तर ऊँचा था गैैर-नागरिकों की अपेक्षा। महिलाएंँ, गुलाम और ‘बारबेरियन’ गैैर-नागरिकों में शामिल थे। कोई व्यक्ति नागरिक हो सकता है या नहीं इसे निर्धारित करने के तरीके संपत्ति (व्यक्ति द्वारा चुकाए जाने वाले करो की मात्रा), राजनीतिक सहभागिता, या विरासत (दोनों अभिभावक पोलिस में जन्मे होने चाहिए) पर आधारित होनेे चाहिए थे। प्राचीन यूनान में मुख्य राजनीतिक इकाई पोलिस (नगर-राज्य) होता था। और नागरिक शेष नगर-राज्य के सदस्य होतेेेे थे। पिछले 500 वर्षों में राष्ट्र-राज्य केे विकास के साथ नागरिकता को एक विशेेष राष्ट्र की सदस्यता के रूप में जाना-जाने लगा हैं। कुछ संस्थाएं राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाती है। जैसेे – व्यापार संगठन, गैर-सरकारी संगठन और मल्टी-नेशनल कारपोरेशनन। कभी-कभी ‘विश्व का नागरिक’ उन लोगों केे लिए प्रयुक्त किया जाता है जो किसी विशेष राष्ट्र के साथ कम संबंध रखते हैं। इसके बजाय उनमें पूरी दुनिया के साथ संबंधित होने की भावना अधिक होती हैं।
आधुनिक समय में,
नागरिकता की नीति ‘जूस सेंगुनिस’ (Jus Sanguinis
) (रक्त का अधिकार) और ‘जूस सोली‘(Jus Soli)
(मृदा का अधिकार) राष्ट्रो के बीच विभाजित है। एक जूस सेंगुनिस नीति जातीयता या वंश के आधार पर नागरिकता देती है और यह यूरोप में प्रचलित एक राष्ट्र-राज्य की अवधारणा से संबंधित हैं। एक जूस सोली नीति हर उस व्यक्ति को नागरिकता देती है जो राज्य के प्रांत विशेष में पैदा हुआ हैं। इस नीति के अनुसरण संयुक्त राज्य सहित अमेरिका के कई देशों मेंं किया जाता हैं।
भारत परिप्रेक्ष्य में देखे तो पाते हैं कि भारत में नागरिकता रक्त का अधिकार और मृदा का अधिकार दोनों मॉडलों से प्राप्त हो जाती हैं। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने के पाँच तरीके हैं –
- जन्म से नागरिकता
- वंश द्वारा नागरिकता
- पंजीकरण द्वारा नागरिकता
- प्राकृतिकीकरण द्वारा नागरिकता
- विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा नागरिकता।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 8 तक प्रत्येक अनुच्छेद में नागरिकों के विशेष वर्ग तय किए गए हैं –
1. अनुच्छेद-5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान लागू होने तक भारत के राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा होता हैं। वह भारत का नागरिक होगा यदि वह निम्न शर्तो में से कम-से-कम एक को पूरी करता हो–
- वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो,
- उसके माता-पिता में से कोई एक भारत के राज क्षेत्र में जन्म लिया हो,
- वह संविधान लागू होने से पहले कम-से-कम 5 वर्षोंतक साधारण तौर पर भारत का निवासी रहा हो।
2.
अनुच्छेद-6 पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आये व्यक्तियों के लिए हैं। इसके अनुसार पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आये हुए किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा।
इस तरह के व्यक्तियों को दो भागों में बांटा गया हैं –
- जो 19 जुलाई, 1948 से पहले भारत आए थे। तथा
- जो 19 जुलाई, 1948 के बाद भारत आए थे।
19 जुलाई, 1948 की तिथि का महत्व यह है कि इसी तिथि से भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत प्रवास के लिए अनुमति-पत्र की प्रणाली शुरू की गई थी।3. अनुच्छेद-7
पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार जिस व्यक्ति ने मार्च, 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया हो, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। लेकिन यदि वह स्थाई रूप से भारत लौटने के लिए अनुमति लेकर वापस आ गया है तो उसकी नागरिकता के संबंध में वही नियम लागू होंगे जो अनुच्छेद-6 में 19 जुलाई, 1948 के बाद भारत आने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं। ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा, जो कम-से-कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद ही किया जा सकेगा।
4. अनुच्छेद–8
उन व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान करता है, जो संविधान के लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे। परंतु वे भारतीय मूल के हैं।
इस अनुच्छेद के अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म अथवा जिसके माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी में से किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम, 1935 द्वारा परिभाषित भारत में हुआ था और वर्तमान में वह व्यक्ति साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा है, वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वह अपने निवास के देश में भारत के राजनयिक परिषद के प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता संबंधी आवेदन प्रस्तुत करता है और उसके आवेदन पर उसकी नागरिकता का पंजीकरण स्वीकार कर लिया जाता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-11 के तहत भारतीय संसद विधि-निर्माण का अधिकार दिया गया हैं। इसी के अंतर्गत वर्ष 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को अभी तक 9 बार संशोधन किया जा चुका है- वर्ष 1957, 1960, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में। वर्तमान में नागरिकता संशोधन कानून-2019 को लेकर देश में काफी विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। यह कानून क्या व्यवस्था करता हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके नागरिकता संशोधन कानून-2019 संसद द्वारा पारित कानून हैं। यह नया कानून व्यवस्था देता है कि 31 दिसंबर, 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, जैन, सिक्ख, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस बिल का प्रकाशन 9 दिसंबर, 2019, हस्ताक्षर 12 दिसंबर, 2019 तथा अनुमति प्रदान की तिथि 12 दिसंबर, 2019 है। इसमें मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, जो विरोध-प्रदर्शन का कारण हो सकता हैं। इस कानून का शीर्षक है- Act No.47 Of 2019, इसे 11 दिसंबर, 2019 को पारित किया गया था। भारत के वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पेश किया था। यह तीन पठनों में पारित हुआ था। पहला पठन 9 दिसंबर, 2019, दूसरा पठन 10 दिसंबर, 2019 और तीसरा और अंतिम पठन संसद द्वारा 11 दिसंबर, 2019 में पारित हुआ था। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोबिंद ने इस बिल पर 12 दिसंबर, 2019 को अपनी स्वीकृति दी। तब अब यह बिल 12 दिसंबर, 2019 से कानून का रूप ले लिया। लेकिन यह कानून 10 जनवरी, 2020 से प्रभावी हुआ।
नागरिकता संशोधन कानून की मुख्य बातें –
इस कानून में कुल-6 धाराएँ हैं। जिसमें धारा-2 के अनुसार अवैध प्रवासी जिसे घुसपैठिया की परिभाषा में स्पष्ट किया गया है कि 31 दिसंबर, 2014 से पूर्व भारत में प्रवेश करने वाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के छ: धर्म के अप्रवासी जैसे- हिंदू, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई समुदाय के व्यक्तियों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। अब सभी गैर-मुस्लिम घुसपैठिए नागरिकता के पात्र हो जाएंगे।
मूल नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा-2 (1) (ख) में अवैध प्रवासी की परिभाषा दी गई हैं, जिसे घुसपैठिए कहा जा सकता है। धारा-1 में नाम तथा विस्तार के बाद नए नागरिकता अधिनियम की धारा-2 से धारा-2 (1) (ख) में परंतु जोड़कर यह अपवाद जोड़ा गया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश के हिंदू, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के ऐसे व्यक्ति जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पूर्व भारत में प्रविष्ट हुआ और केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट तथा विदेशी विषय अधिनियम से छूट दी गई है तो वह अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। लेकिन यह धारा पूर्वोत्तर के अनुसूची-6 और इनर लाइन वाले राज्यों पर नहीं लागू होगी।