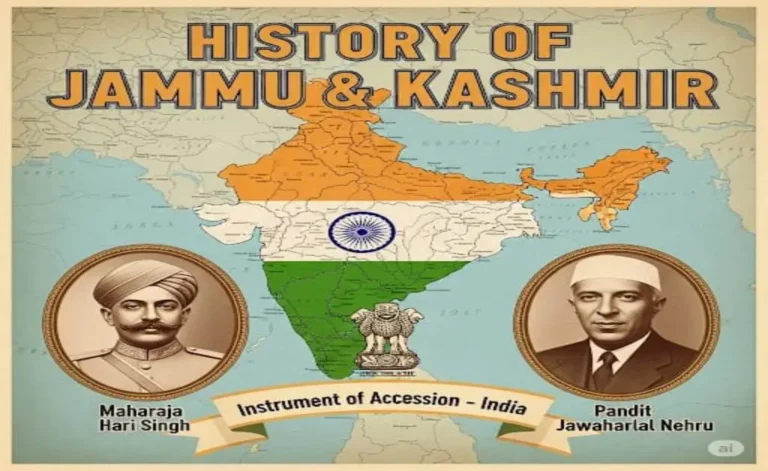What are the main sources of indian constitution – भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत क्या हैं?
26 नवंबर, 1949 को पारित और 26 जनवरी, 1950 से लागू संविधान के लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह संसार के सभी देशों के संविधानों की अच्छी बातों को अपने में शामिल कर लेता। डॉ॰ एम॰ पी॰ शर्मा ने कहा है कि “हमारे संविधान निर्माता को प्रयोजन एक मौलिक और अनूठा (unique) संविधान बनाना नहीं था। वे तो एक अच्छा और व्यवहारिक संविधान बनाना चाहते थे। अतः उन्होंने संसार के अनेक देशों के संविधानों की श्रेष्ठ बातों को लेना उचित समझा।” इस प्रकार भारतीय संविधान ने अनेक स्रोतों से सहायता ली हैं।
भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत (Main sources of Indian Constitution) –
भारत के संविधान पर विदेशी संविधानों में सबसे अधिक प्रभाव ब्रिटिश संविधान का पड़ा हैं। इसका कारण यह है कि ब्रिटेन का अलिखित संविधान संसार के प्राचीनतम संविधानों में से हैं और उसने संसार के प्रायः सभी देशों की शासन व्यवस्था को बहुत हद तक प्रभावित किया है। जिन देशों के संविधानों से हमारे संविधान प्रभावित हैं या जिनसे जो व्यवस्थाएँ ली गई हैं, उन्हें हम निम्न प्रकार से देखेंगे –

1. ब्रिटिश संविधान से –
- सरकार का संसदीय स्वरूप,
- कानून का शासन,
- कानून निर्माण की विधि,
- लोक सभा के अध्यक्ष पद एवं उनकी भूमिका,
- सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय।
2. कनाडा के संविधान से –
- एक अर्ध-संघात्मक सरकार का स्वरूप,
- सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था,
- अविशिष्ट अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है।
3. फ्रांस के संविधान से –
- स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत।
4. जर्मनी (वाइमर) के सिद्धांत से –
- राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार लिया गया हैं।
5. अमेरिका के संविधान से –
- मौलिक अधिकारों की सूची,
- सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय की स्वतंत्रता तथा न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार लिया गया हैं।
6. आयरलैंड के संविधान से –
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्यवस्था,
- राज्यसभा तथा राज्य विधान परिषद में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों का मनोनयन।
7. ऑस्ट्रेलिया के संविधान से –
- समवर्ती सूची का सिद्धांत।
8. दक्षिण अफ्रीका के संविधान से –
- संविधान संशोधन पद्धती।
9. 1935 के भारत सरकार अधिनियम से –
उपर्युक्तत विदेशी संविधानों की तरह ही भारत के संविधान पर 1935 के भारत सरकार अधिनियम का प्रभाव सबसे अधिक गहरा हैं। डॉ॰ जेनिंग्ज (Jennings) ने तो यहांँ तक कहा है कि, “भारतीय संविधान का उद्भव सीधे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ है और इसके बहुत से प्रावधान वस्तुतः ज्यों के त्यों संविधान में शामिल कर लिए गए हैं।” भारतीय संविधान के अनुच्छेद 251, 256, 352, 353 और 356 अधिनियम 1935 की धारा 107, 126, 102 और 92 पूरी तरह नकल हैं। इस समानता की वजह से ही डॉ॰ पंजाबराव देशमुख ने तो यहांँ तक कह डाला है कि “नवीन संविधान और 1935 के अधिनियम में व्यस्क मताधिकार (Adult franchise) को छोड़कर और कोई अंतर नहीं हैं।”यद्यपि डॉ॰ देशमुख का यह कथन सही नहीं है, फिर भी 1935 के अधिनियम की लगभग 200 धाराओं की उसी तरह या उनके मूल सिद्धांतों में परिवर्तन किए बगैर केवल शब्द और वाक्यों में रद्दोबदल कर नवीन संविधान में शामिल कर लिया गया हैं।
संविधान के अन्य स्रोत (Other source of the constitution) –
उपर्युक्त स्रोतों के अलावे कुछ अन्य स्रोत भी हैं जिसे हम निम्नलिखित रुप में अध्ययन करेंगे-
1. अभिसमय और प्रथाएंँ (Conventions and usages) –
अभिसमय और प्रथाएंँ प्रायः संविधान का यह अलिखित भाग होती है जो क्रमिक रूप से किसी भी देश में बदलती हुई परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित होती हैं। ब्रिटिश संविधान तो अभिसमयों और प्रथाओं पर आधारित हैं। सर आईवर जेनिंग्ज ने इस संबंध में कहा है कि, “अभिसमय कानून के अस्थिपंजर पर मांस का कार्य करती हैं।”
2. संविधान सभा की कार्यवाही (Constituent assembly debates) –
भारतीय संविधान के लिखित होने और उच्चतम न्यायालय द्वारा उसकी व्याख्या की व्यवस्था होने के बावजूद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जबकि संविधान की किसी लिखित व्यवस्था का सही अर्थ समझ पाना बड़ा कठिन हो रहा हो। उस अवस्था में उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या करते समय संविधान सभा की कार्यवाही विवरण को देखकर संबंधित व्यवस्था की मूल भावना को ठीक प्रकार से समझा सकता है। तब निर्णय भी दे सकता हैं। जैसे- गोपालन बनाम मद्रास राज्य संबंधी मुकदमें में संविधान सभा की कार्यवाही के विवरण का उदाहरण दिया गया था। अतः संविधान सभा की कार्यवाही विवरण भी भारतीय संविधान का एक उपयोगी स्रोत बन जाती हैं।
3. न्यायिक निर्णय (Judicial decision) –
किसी भी लोकतांत्रिक देश में वहां की न्यायपालिका द्वारा महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों द्वारा किए गए निर्णय संविधान के स्रोत का कार्य करते हैं। भारत पर यह कथन पूरी तरह लागू होती हैं। 24 अप्रैल 1973 को संविधान के 24वें, 25वें और 29वें संशोधन अधिनियमों की वैधता संबंधी मुकदमे पर अपना निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय ने यही कार्य किया। दूसरी ओर देखे तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार के मुकदमों में अपने द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णय से उच्चतम न्यायालय ने संविधान की व्याख्या करके उसे समृद्ध बना दिया हैं। अतः न्यायिक निर्णय भी भारतीय संविधान के अन्य स्रोत हैं।
4. संवैधानिक विशेषज्ञों के विचार (Views of Jurists) –
सभी देशों में संविधानों पर महत्वपूर्ण टिकायें लिखने वाले व्यक्तियों के विचारों का बहुत आदर किया जाता हैं। जैसे- ब्रिटेन के ब्लैकस्टोन (Blackstone), डायसी (Diecy), जेनिंग्ज (Jennings) और सर अरशाइन मे (Sir Ershine May) के विचारों का न केवल ब्रिटेन में बल्कि भारत सहित अन्य देशों में भी बहुत आदर किया गया हैं और संविधान की व्यवस्थाओं को समझने के प्रयास भी हुए हैं। अतः वे भी भारतीय संविधान के उल्लेखनीय स्रोतों में से एक हैं।
5. संविधान के संशोधन (Amendments of the constitution) –
संविधान संशोधन भी संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार (Right to property) आज उस पर नहीं हैं। जैसे उसकी संविधान लागू करते समय व्यवस्था की गई थी। इस परिवर्तन में संविधान के पहले, चौथे, 17वें, 25वें और 29वें संशोधन अधिनियम का महत्वपूर्ण भाग रहा हैं।
निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की रचना और उसके विकास में अनेकानेक स्रोतों का योगदान रहा हैं। उसे किसी एक स्रोत पर पूरी तरह निर्भर नहीं समझा जा सकता। विश्व के अनेक देशों के संविधानों, 1935 के भारत सरकार अधिनियम और अभिसमय, प्रथाओं, न्यायिक निर्णयों, संविधान सभा की कार्यवाही, संवैधानिक विशेषज्ञों की टिकाओं आदि सभी ने उसका कलेवर बढ़ाने में सहायता दी हैं और ठीक प्रकार से समझे बिना भारतीय संविधान को समझ पाना कठिन होगा।